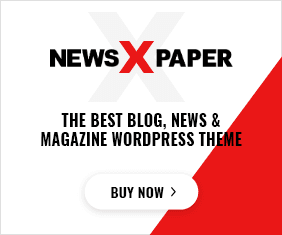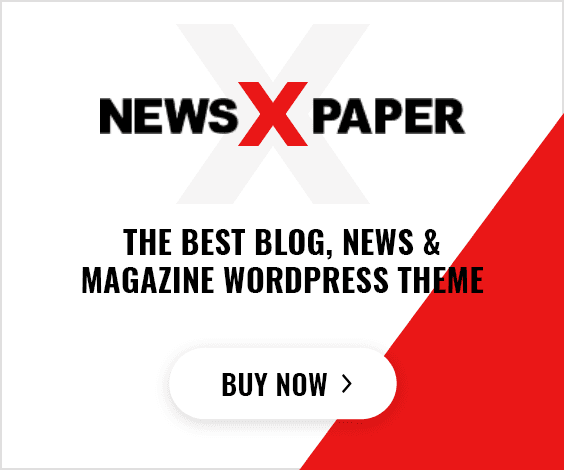वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए चुनौतियों से भरे इस दौर में पारंपरिक चिकित्सा की ताक़त एक बार फिर सम्मान और मान्यता पा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हालिया आँकड़े बताते हैं कि 194 सदस्य देशों में से 170 देश किसी न किसी रूप में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था का हिस्सा बनाए हुए हैं। सस्ती, सुलभ और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होने के कारण अरबों लोगों के लिए यह प्रणाली आज भी अनिवार्य है। पर इसका महत्व केवल रोग उपचार तक सीमित नहीं है। यह जैव विविधता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका की स्थिरता से भी गहराई से जुड़ा है।
वैश्विक बाज़ार और भारत की भूमिका
दुनिया भर में पारंपरिक औषधियों का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2025 तक यह 583 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा। चीन का पारंपरिक चिकित्सा उद्योग 120 अरब डॉलर से अधिक है, ऑस्ट्रेलिया का हर्बल उद्योग 4 अरब डॉलर के आसपास है और भारत का आयुष क्षेत्र (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) 43 अरब डॉलर से ऊपर पहुँच चुका है। यह आँकड़े दर्शाते हैं कि स्वास्थ्य सेवा का फोकस अब केवल लक्षणों के उपचार से हटकर समग्र और निवारक दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है।
आयुर्वेद का भारतीय पुनर्जागरण
भारत इस बदलाव का अग्रदूत बनकर उभरा है। पिछले एक दशक में आयुष क्षेत्र ने आठ गुना विस्तार दर्ज किया है। निर्माण क्षेत्र की आय 2014-15 में लगभग 21,600 करोड़ रुपये थी, जो अब 1.37 लाख करोड़ तक पहुँच गई है। वहीं सेवाओं के क्षेत्र का राजस्व 1.67 लाख करोड़ रुपये है। आयुष और हर्बल उत्पादों का निर्यात अब 150 से अधिक देशों में हो रहा है, जिसकी कुल क़ीमत 1.5 अरब डॉलर से ज़्यादा है।
राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय (2022-23) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 95 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 96 प्रतिशत लोगों ने आयुष के बारे में जानकारी रखी, जबकि आधी से अधिक आबादी ने बीते वर्ष किसी न किसी आयुष पद्धति का उपयोग किया। आयुर्वेद विशेष रूप से जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए पसंदीदा विकल्प बनकर उभरा है।
परंपरा और विज्ञान का संगम
वैश्विक स्तर पर विश्वसनीयता के लिए वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक हैं और भारत इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है। ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद और अन्य शीर्ष शोध संस्थान पारंपरिक चिकित्सा की वैज्ञानिक जाँच, गुणवत्ता मानक और आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकृत शोध पर कार्यरत हैं।
भारत का आयुष मंत्रालय 70 से अधिक अंतरराष्ट्रीय समझौतों, विदेशी विश्वविद्यालयों में चेयर्स, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जैसी पहलों के माध्यम से इसे वैश्विक मान्यता दिला रहा है। डिजिटल मंच जैसे नमस्ते पोर्टल और द्रव्य प्लेटफ़ॉर्म आयुर्वेद को बिग डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़कर साक्ष्य आधारित चिकित्सा को नई दिशा दे रहे हैं।
आयुर्वेद: मानव और प्रकृति का संतुलन
आयुर्वेद का दर्शन संतुलन पर आधारित है मन और शरीर का, मानव और प्रकृति का, उपभोग और संरक्षण का। यही कारण है कि इस वर्ष 23 सितंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का विषय रखा गया: “लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद”। यह संदेश स्पष्ट है कि स्वास्थ्य केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण, कृषि, पशु चिकित्सा और पारिस्थितिकी का भी अभिन्न हिस्सा है।
आगे की राह
भविष्य में पारंपरिक चिकित्सा को टिकाऊ और प्रभावी बनाए रखने के लिए तीन स्तंभ ज़रूरी हैं वैज्ञानिक प्रमाण, नैतिक मानक और समाज की सक्रिय भागीदारी। भारत ने इस दिशा में जो रास्ता दिखाया है, वह न केवल विरासत और नवाचार का संगम है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक अवसर का भी नया अध्याय है।
आयुर्वेद दिवस का दसवाँ वर्ष केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य नीति में समग्रता और स्थिरता की दिशा में आह्वान है। यदि हम परंपरा और विज्ञान का संतुलित समन्वय कर पाए, तो पारंपरिक चिकित्सा न केवल आज की बीमारियों का समाधान देगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य भी सुनिश्चित करेगी।